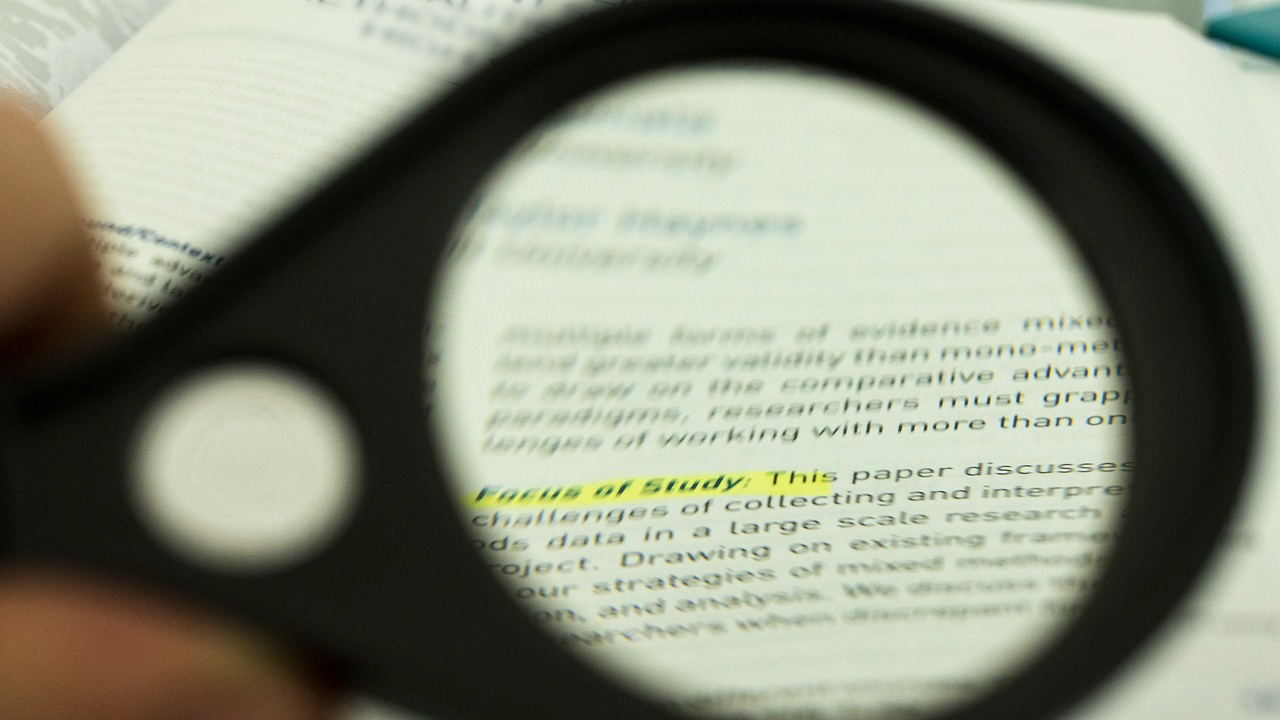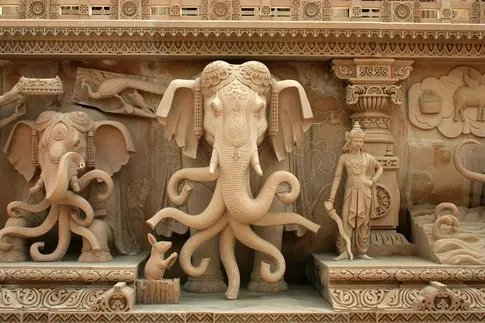संशोधन के प्रकार तथा वर्गीकरण
शोध के प्रकार –
अनुसंधान के क्षेत्र में संशोधन के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। तथापि अनुसंधाताओं ने संशोधन के कुछ प्रकार निर्धारित किया है । अनुसंधान के प्रकार शोध के अलग-अलग क्षेत्र से संबंधित है जिनमें विज्ञान, समाज, तकनीकी, साहित्य, भाषा आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं । शोध में संशोधन के प्रकारों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है –
क. प्रयोजन के अनुसार – 1. वर्णनात्मक 2. अन्वेषणात्मक 3. स्पष्टीकरणात्मक
ख. हेतु के अनुसार – 1. शुद्ध अथवा मूलभूत 2. अनुप्रयुक्त अथवा कार्यात्मक
ग. तथ्यों के वैशिष्ट्य के अनुसार – 1. गुणात्मक 2. संख्यात्मक
घ. तुलनात्मकता के अनुसार – 1. रेखावृत्तीय 2. तुलनात्मक
ङ. अन्य – 1. काल्पनिक 2. प्रायोगिक 3. ऐतिहासिक 4. प्रयोगशाला संबंधित इत्यादि।
क. प्रयोजन के अनुसार –
प्रत्येक शोध का एक विशिष्ट प्रयोजन होता है वह प्रयोजन किसी फल की अभिलाषा का मूल है। फल प्राप्ति के लिए प्रयोजन के विविध आयाम हो सकते हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में प्रयोजन की दृष्टि से किया गया शोध भी अलग-अलग स्वरूपों में दिखाई पड़ता है जिसके कुछ भेद यहां किए गए हैं।
- वर्णनात्मक संशोधन – वर्णनात्मक संशोधन व्याख्या का एक उत्तम साधन है। इस विधा में शोध को पूर्ण रूप से शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। व्याख्या करते समय शोध में प्राप्त अनुभव एवं कार्यों का भी शब्दशः वर्णन किया जाता है। शोधकर्ता वर्णन करते समय विषय से संबंध प्रत्यय गुण एवं दोष को अपने शब्दों में निरूपित करता है तथा अपने विषय को विस्तार देते हुए विषय की उपयोगिता को स्पष्ट करता है। संशोधन की इस विधा में शोधकर्ता प्राप्त अनुभवों को सारणीबद्ध करके एक प्रगति विवरण के रूप में प्रस्तुत करता है तथा उस विवरण में विषय की आरंभिक अवस्था से वर्तमान अवस्था तक का सफर सरल एवं सुबोध शब्दों में प्रस्तुत करता है। भारत की जनगणना वर्णनात्मक संशोधन का एक उत्तम उदाहरण है। जिसमें जनगणना की पूर्वस्थिति, मध्यस्थित तथा वर्तमान स्थिति का सविस्तर विवरण तैयार किया जाता है और यह विवरण राष्ट्रहित में समाजहित में तथा जनहित में लाभकारी सिद्ध होता है। इसी प्रकार शोध का यह प्रकार राष्ट्र के प्रत्येक अवयव के लिए लाभकारी सिद्ध हो इस दृष्टि से शोध कार्य किया जाना चाहिए। यह संशोधन विषय के नियोजन और संशोधन के द्वारा अनुमानित निष्कर्ष तैयार करने के लिए सहायक होता है। विषय के वर्णन के द्वारा ही विषय का विस्तार प्राप्त होता है और गहन अध्ययन करके की गई व्याख्या निष्कर्ष प्रताप का सहायक मार्ग बनती है। शोध कार्य की किसी भी घटना को सविस्तर परखने के लिए वर्णनात्मक संशोधन से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। शोध के वर्णन में छोटी से छोटी घटना एवं तथ्यों का उल्लेख किया जाता है जिसके द्वारा विचार विमर्श करते हुए विषय की गंभीरता और उसके द्वारा होने वाले लाभ को प्रमाणित सिद्ध किया जा सके। सामाजिक क्षेत्र में तथा व्यावसायिक क्षेत्र में किसी घटना के निरंतर घटित होने पर उसके परिणाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्णनात्मक संशोधन का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा घटित हुई घटना का विस्तार से वर्णन कर प्रत्येक अंश को परखने का अवसर प्राप्त होता है और उचित निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। इस संशोधन में लोगों की विचारधारा एवं दृष्टिकोण के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है यह संकलन कभी-कभी असत्य भी सिद्ध हो सकता है क्योंकि घटना के प्रति लोगों का दृष्टिकोण कैसा है इस पर हमारा अंकुश नहीं होता।
- अन्वेषणात्मक संशोधन – संशोधन का यह प्रकार खोज से जुड़ा है इसके अंतर्गत समस्या को अलग-अलग दृष्टिकोण से जांच वह पर परखा जाता है। इसके द्वारा समस्या के समाधान के लिए विविध अर्थबोध और समाधान की दिशाएं प्राप्त होती है। यह संशोधन कम से कम तथ्यों वाला होने के कारण बौद्धिक स्तर को बढ़ाने वाला होता है क्योंकि तथ्यों की कमी के कारण वैचारिक क्षमता का अधिक होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता को समस्या की गहराई और परिस्थिति का काम ज्ञान होता है अथवा कभी-कभी कोई अनुमान ही नहीं होता। इस संशोधन के कार्य में आधे से ज्यादा समय अनुमान के मार्ग पर ही खर्च होता है। इसके अंतर्गत ऐसे विषय होते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में देखना या अनुभव करना संभव नहीं होता है अतः उनका अनुमानित विश्लेषण किया जाता है तत्पश्चात अन्वेषण की प्रक्रिया के द्वारा किसी निर्णय को प्राप्त किया जाता है। इस संशोधन के विषय कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे सागर की गहराई में प्राप्त होने वाले जीव और अमूल्य रत्न आदि, भूमि के नीचे प्राप्त होने वाली संरचनाएं तथा किसी प्रदेश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण इत्यादि। यह संशोधन बार-बार घटित होने वाली घटनाओं की मूल करण प्रक्रिया को जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जैसे- शैक्षणिक पद्धति की व्यवस्था में कमी, सरकारी विभागों का लचीलापन व ग्रामीण क्षेत्र की दरिद्र स्थिति इत्यादि सामाजिक क्षेत्र के संशोधन के लिए यह संशोधन विद्या अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- स्पष्टीकरणात्मक संशोधन– इस संशोधन के अंतर्गत घटनाओं के कारणों का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है। घटित हुई घटना का विश्लेषण कर उसके समस्त अनुमानित कारणों को एकत्रित करके स्पष्टीकरण के द्वारा निश्चित कारण को प्राप्त करना यह इस अनुसंधान की प्रक्रिया है। यह अनुसंधान सुविधा भौगोलिक स्तर पर अधिक उपयोगी मानी गई है जैसे की किसी क्षेत्र में भूकंप की निरंतर स्थिति का स्पष्टीकरण करना। इसके माध्यम से वस्तुओं की गुणवत्ता को भी जांचा जाता है और कमी आने पर स्पष्टीकरण के माध्यम से उचित समाधान भी प्राप्त किया जाता है। यह अनुसंधान विद्या प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसंधान के अंतर संबंध को स्पष्टीकरण के द्वारा स्थापित करना है जिससे कि अनुसंधान को उचित निष्कर्ष प्राप्त हो सके और वह अनुसंधान समाज के कल्याण का कारण बने।
ख. हेतु के अनुसार – प्रायः कोष की दृष्टि से प्रयोजन और हेतु समान अर्थ वाले हो सकते हैं किंतु प्रयोग दृष्टि से दोनों में कुछ भेद आवश्यक होता है। प्रयोजन वह कार्य है जो शोध में प्रवृत्ति पैदा करता है और हेतु शोध के निष्कर्ष में सहायक होते हैं। शोध के कुछ मूलभूत हेतु हैं जीनसे संशोधन को गति प्राप्त होती है और निर्णय तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त होता है।
- शुद्ध अथवा मूलभूत संशोधन – शुद्ध संशोधन शोध कार्य की मूल संकल्पना है जिसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है अतः इसे सैद्धांतिक संशोधन भी कहा जा सकता है। इस संशोधन का संबंध नैसर्गिक घटना तथा शुद्ध व्यवहार वाले संशोधन से होता है जिसमें मूल तथ्य प्राप्त कर शोध को गति प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत ऐसे विषयों का चयन किया जाता है जिससे संबंधित पूर्ण जानकारी नहीं होती है अथवा छुपी हुई होती है। इस प्रकार सिद्धांतों के मूल संकलन के द्वारा पूर्व सिद्धांतों पर प्राप्त घटनाक्रम को परख कर सैद्धांतिक संशोधन आरंभ किया जाता है। मूल संशोधन अपने परिणाम स्वरूप समाज को एक विशेष सिद्धांत प्रदान करता है जो की वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा को और समाज को गति प्रदान करता है। वर्तमान में प्राप्त गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अथवा अन्य कोई वैज्ञानिक सिद्धांत इस प्रकार के संशोधन का उदाहरण है। शुद्ध संशोधन को उचित एवं व्यावहारिक महत्व की दृष्टि से उच्चतम गुणवत्ता वाला शोध कार्य करने के लिए मूलभूत संशोधन को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। (अ) नवीन सिद्धांत का शोध – इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपने शोध कार्य में कल्पना और प्रतिभा के आधार पर ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है जो आज से पहले विज्ञान के किसी क्षेत्र में उल्लिखित नहीं थे। यह सिद्धांत विज्ञान, तकनीकी तथा सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करके विकास के क्रम में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आइंस्टीन न्यूटन इत्यादि के सिद्धांत इस संशोधन विद्या के उदाहरण कहे जा सकते हैं। (आ) पूर्व प्रचलित सिद्धांत का विकास – सैद्धांतिक संशोधन का यह प्रकार निरंतर हो रहे बदलाव को संकेतित करता है। विज्ञान के क्षेत्र में अनेकों शोध हुए हैं जो कि समय के साथ अपने सिद्धांतों में परिवर्तन को प्राप्त कर रहे हैं ये परिवर्तन सामाजिक दृष्टि एवं तकनीकी दृष्टि से स्वीकार किए जाते हैं उन परिवर्तनों को सैद्धांतिक रूप से समाज के सामने स्थापित करना और उनकी उपयोगिता को बरकरार रखना इस विधा का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत मूल सिद्धांतों का पुनः पुनः विश्लेषण कर सिद्धांत के परिवर्तन के कारण को जानना और नवीन शोध के द्वारा तथा शोधकर्ता की बुद्धिमत्ता कौशल के द्वारा सिद्धांत को पुनः स्थापना करना इस शोध के अंतर्गत आता है। संशोधन के इस स्वरूप को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो शोध पूर्व में किया जा चुका है अथवा जिनका स्पष्टीकरण और व्याख्या हमें प्राप्त है उसका वर्तमान युग में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, उसमें किन परिवर्तनों की आवश्यकता है इत्यादि विषयों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में किए गए शोध की पुनः स्थापना करना इस शोध विधा का कार्य है।
- अनुप्रयुक्त अथवा कार्यात्मक संशोधन – इसका उपयोग त्वरित क्रियान्वयन के लिए किया जाता है अर्थात एहसास संशोधन जो ज्ञान विस्तार के लिए किसी भी स्वरूप में व्यावहारिक उपयोग के लिए त्वरित काम में लिया जा सके वह अनुप्रयुक्त अथवा कार्यात्मक संशोधन कहलाता है। इस संशोधन विद्या में बौद्धिक उत्सुकता और ज्ञानवर्धन के कार्यों पर विशेष भार दिया जाता है। मानवी जीवन हर समय किसी न किसी समस्या से ग्रसित होता है मनुष्य को जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अनुप्रयुक्त संशोधन की आवश्यकता होती है जिससे वह अपनी समस्याओं का तुरंत निराकरण कर सके। आता है अनुप्रयुक्त संशोधन समस्या निवारण के लिए भी उपयुक्त है। जब शुद्ध संशोधन का विकसित रूप सिद्धांतों के माध्यम से समाज के सामने प्रतिपादित किया जाता है तो उसे सिद्धांत का क्रियान्वयन स्वरूप तैयार करने का कार्य अनुप्रयुक्त संशोधन की सहायता से किया जाता है। सामाजिक स्तर पर सिद्धांतों का क्रियान्वयन स्वरूप एवं व्यावहारिक स्तर पर जीवन पर पड़ने वाले उन सिद्धांतों के फल का प्रतिपादन करना अनुपयुक्त संशोधन का कार्य है अतः अनुपयुक्त संशोधन अन्य संशोधन विधाओं का भी सहयोग करने में सक्षम है। समाज में औद्योगिक स्तर पर तथा सामाजिक स्तर पर अनुप्रयुक्त संशोधन का बार-बार प्रयोग किया जाता है। मनुष्य जीवन में क्रियात्मक संशोधन को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। यह संशोधन प्रत्येक क्षेत्र में दैनंदिन कार्यों के नियोजन के लिए प्रयुक्त किया जाता है अतः इसे उपयोजित संशोधन भी कहा गया है।
ग. तथ्यों के वैशिष्ट्य के अनुसार –
शोध करते समय अनेक प्रकार के तथ्य सामने आते हैं। तथ्यों को शोध के अनुसार विभाजित कर उनके वैशिष्ट्य को समझ कर तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। तथ्यों के उचित विश्लेषण के लिए उनकी विशेषताओं के आधार पर शोध कार्य को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है।
- गुणात्मक संशोधन – शोध कार्य के तथ्यों की गुणवत्ता को रखने का कार्य इस संशोधन के द्वारा किया जाता है। गुणात्मक संशोधन तथ्यों की उपयोगिता एवं शोध में उनके गुणों का विश्लेषण करता है। यह संशोधन विस्तृत व्याख्या के समान नहीं होता है इसके अंतर्गत कम शब्दों में तथ्यों की बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जिससे कि शोध की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। गुणात्मक संशोधन में शोध कार्य से संबंधित सर्वेक्षण में भी लोगों के मतों और उनकी व्यक्तिनिष्ठ क्रियाओं पर बारीकी से अध्ययन किया जाता है जिससे कि शोध की गुणवत्ता को उचित प्रकार से परखा जा सके। गुणात्मक संशोधन का सामाजिक महत्व भी व्यापक है । समाज में कार्य करने वाले पारिश्रमिक वर्ग तथा व्यावसायिक वर्ग के मध्य अंतर्संबंध को विवाद रहित बनाए रखने के लिए समय-समय पर गुणात्मक संशोधन के द्वारा सामाजिक सर्वेक्षण करके कार्यों का एवं व्यवहार का गुणवत्ता को परिशीलन किया जाता है। वर्तमान समय में कई कंपनियां साक्षात्कार के माध्यम से श्रमिकों का चयन करती है। जिसमें कंपनी तथा श्रमिक के मध्य कार्य, समय व वेतन इत्यादि की सविस्तृत चर्चा की जाती है तथा श्रमिक की गुणवत्ता को भी जांच परखकर देखा जाता है। चयन की यह पद्धति गुणात्मक संशोधन के द्वारा निर्मित की गई है। गुणात्मक संशोधन समाज के प्रत्येक वर्ग की सम स्थिति के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह संशोधन समाज में बैलेंस बनाने का कार्य करता है जिससे कि उच-नीच के भाव एवं किसी भी कार्य की हीन दृष्टि को बढ़ावा नहीं मिलता है।
संख्यात्मक संशोधन – संशोधन का यह प्रकार संख्या के आधार पर शोध कार्य को गति प्रदान करता है। वस्तुतः इस संशोधन का आधार मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर करता है। अतः इस संशोधन में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विशेष महत्व है। इस संशोधन के माध्यम से तथ्यों का संख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है जिसके अंतर्गत लाभ – हानि को स्पष्ट रूप से परखा जाता है। यह संशोधन व्यवसाय, कृषि तथा मूल्य मापन संबंधी संस्थाओं के लिए अतिव महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से जनसंख्या का उतार-चढ़ाव, कृषि में उत्पादन, व्यवसाय का विकास, उत्पन्न, खर्च, आयात व निर्यात इत्यादि विश्लेषण संख्यात्मक दृष्टि से किया जा सकते हैं। संशोधन की यह विधा एक कालावधि निश्चित कर तथ्यों के आंकड़े तैयार कर सकती है जिससे कि पूर्व के वर्षों में हुए लाभ और हानि को समझ कर कार्य की रूपरेखा में उचित बदलाव किया जा सके। इस प्रकार वस्तुओं के आयात निर्यात कम को भी व्यवस्थित किया जा सकता है।
घ. तुलनात्मकता के आधार पर – शोध कार्य में किसी विषय से संबंधित प्राप्त तथ्यों में प्रमाणिकता के आधार पर गुणवत्ता का निर्णय करने के लिए तुलनात्मक संशोधन का सहयोग लिया जाता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक तथ्यों का परस्पर तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है । यह तुलनात्मक अध्ययन तथ्यों को विविध रूपों में विभाजित कर विविध प्रकार से परिशीलित करता है। तुलनात्मक संशोधन को दो प्रकार से समझा जा सकता है –
- रेखा वृत्तीय संशोधन – यह संशोधन कुछ-कुछ संख्यात्मक संशोधन के जैसा दिखाई पड़ता है किंतु इस संशोधन में किसी विशेष कालावधि में हुए विकास को रेखांकित किया जाता है अन्य तथ्यों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता जबकि संख्यात्मक संशोधन सभी दिशाओं में समान कार्य करता है। यह संशोधन घटनाओं में हुए बदलाव के मुख्य कारणों को समझ कर उनका विश्लेषण करता है और यह बदलाव कि कालावधि में से आरंभ और विकास के समय का विश्लेषण कर को इसका आरेख तैयार करता है जिससे कि बदलाव का उचित अभ्यास हो सके और महत्वपूर्ण घटकों को समझा जा सके। जैसे की विगत 25 वर्षों में किसी प्रदेश की वर्षा की जानकारी एकत्रित करना, विगत 10 वर्षों में किसी राज्य की व्यापारिक स्थिति को रेखांकित करना तथा किसी राज्य में 20 वर्षों से विलंबित कार्यों को रेखांकित करना इत्यादि विश्लेषण इस संशोधन में किए जाते हैं।
- तुलनात्मक संशोधन – इस संशोधन विधा में तथ्यों को घटकों में विभाजित कर अलग-अलग दृष्टिकोण से अभ्यास किया जाता है। संशोधन के इस स्वरूप में तथ्यों का भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक समूह बनाकर अलग-अलग दृष्टिकोण से वैशिष्ट्यपरक तुलनात्मक अभ्यास किया जाता है। भौगोलिक स्थिति में दो प्रदेशों का तुलनात्मक विचार करते हुए शोध किया जाता है इसी प्रकार सांस्कृतिक स्थिति में दो अलग-अलग जनजातीय की तुलना करते हुए विचार किया जाता है। तुलनात्मक संशोधन के घटक शोध कार्य के क्षेत्र और सामाजिक स्थिति पर निर्भर करते हैं इसके अंतर्गत आर्थिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति इत्यादि समाहित है। जब दो क्षेत्र में तुलना की जाती है तो उन दोनों क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को जांच परख कर तथ्य तैयार किए जाते हैं तदुपरांत उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या एवं उनके रहन-सहन को तथ्यों के माध्यम से विश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक तुलनात्मक संशोधन अपने अलग घटकों के माध्यम से शोध कार्य को परिपूर्ण करता है तथा गुणवत्ता को प्रदान करता है।
ङ. अन्य संशोधन – संशोधन क्षेत्र में कुछ शोध कार्य ऐसे भी होते हैं जिनको पूर्व उल्लिखित विधाओं में समाविष्ट करना कठिन होता है। ये शोध कार्य अन्य संशोधन कार्यों की अपेक्षा अलग होते हैं अतः संशोधन के कुछ विशेष प्रकार किए गए हैं जो इस खंड में प्रस्तुत किए गए हैं।
- संकल्पनात्मक संशोधन – यह शोध कार्य कल्पना से चुने गए विषय और सिद्धांत से संबंधित होता है। इस शोध के अंतर्गत समाज की किसी ऐसी स्थिति को स्पष्ट किया जाता है जो की अनुमानित रूप से भविष्य में घटित हो सकती है। यह संशोधन अनुमान प्रमाण के आधार पर आगे बढ़ता है और भविष्य में आने वाली कठिनाई का समाधान खोजने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त किसी विषय के प्राथमिक विकास के लिए संकट की गई जानकारी के आधार पर किया गया संशोधन भी संकल्पनिक संशोधन कहलाता है। वस्तुतः संकल्पनिक संशोधन ऐतिहासिक एवं पुरातत्व विषयक शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों ही विषयों में आरंभिक जानकारियां कल्पना के आधार पर तैयार की जाती है इसके उपरांत उस अनुमान के अनुरूप कार्य करते हुए मुख्य तथ्यों तक पहुंच जाता है। इस संशोधन में किसी भी विषय की मूलभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए कल्पना शक्ति का ही उपयोग किया जाता है तथा कुछ सिद्धांत भी काम आते हैं किंतु शास्त्रीय सिद्धांतों का इस शोध कार्य में प्रायः अभाव देखा गया है।
- प्रायोगिक संशोधन – इस संशोधन में प्रयोग के आधार पर विषयों को समझा जाता है। यह शोध कार्य तथ्यों पर आधारित होता है। तथ्यों तथा उपलब्ध जानकारी के अनुरूप निष्कर्ष प्राप्त कर शोध कार्य को गति दी जाती है। प्रायोगिक संशोधन में निरीक्षण के लिए पुनः पुनः प्रयोग विधि का उपयोग किया जाता है। संशोधन कल में प्राप्त तथ्यों को सिद्ध करने के लिए तदनुकूल जानकारियां जमा की जाती है और उनका परीक्षण किया जाता है। प्राप्त जानकारियों पर प्रयोग करके अथवा अनुभव के आधार पर अभ्यास रूप में शोध कार्य को बल दिया जाता है।
- सर्वेक्षण संशोधन – किसी भी शोध कार्य में मूलभूत जानकारी को एकत्रित करने के लिए सर्वेक्षण का सहयोग लिया जाता है । पृथ्वी पर प्राप्त विविध घटकों के आंतरिक संबंध को समझने के लिए भी सर्वेक्षण संशोधन उत्तम साधन है। इसके माध्यम से सूक्ष्म अध्ययन के लिए विशिष्ट जानकारियां प्राप्त की जाती है जो की शोध कार्य को प्रमाणिकता प्रदान करती है। सर्वेक्षण संशोधन के अंतर्गत प्रश्नावली, चर्चा व मीटिंग इत्यादि के आधार पर लोगों से परस्पर मिलकर निरीक्षण किया जाता है और प्राप्त जानकारी को संकलित कर शोध कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। सर्वेक्षण संशोधन विषय की मूलभूत जानकारी को प्रदान करता है अतः विषय से संबंधित प्रत्येक घटक का इसमें सहभागी होना आवश्यक है। जैसे कि अगर सर्वेक्षण का विषय सामाजिक है तो समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति तथा प्रत्येक स्तर का व्यक्ति सर्वेक्षण का अंग बने यह अनिवार्य होगा। अगर इस प्रकार के संशोधन में किसी भी वर्ग को या व्यक्ति विशेष को छोड़ दिया जाए तो प्राप्त निष्कर्ष पूर्ण रूप से परिष्कृत नहीं होंगे और उन्हें प्रामाणिक नहीं कहा जा सकेगा।
- कृति संशोधन – यह संशोधन शोध कार्य की रूपरेखा के आधार पर कार्य करता है। किसी समस्या के समाधान के लिए नियमित पद्धति, नियमों का अनुप्रयोग एवं शास्त्रीय विधि से किया गया शोध का नियोजन जिस प्रकार की रूपरेखा तैयार करता है वह कृति संशोधन कहलाता है। वर्तमान काल में जन्म ले रही समस्या का भविष्य में होने वाले परिणामों पर विचार करके उसके समाधान की रूपरेखा तैयार करना इस संशोधन का मूलभूत कार्य है। उदाहरण के लिए आने वाले 10 वर्षों में प्रदेश में होने वाली जनसंख्या वृद्धि पर विचार कर भविष्य में सामाजिक परिस्थितियों को किस प्रकार नियोजित किया जा सकता है तथा समाज में अव्यवस्था ना हो इसके लिए क्या-क्या प्रयास किया जा सकते हैं इन सभी विषयों पर विचार कर एक उचित रूपरेखा तैयार करना एवं समस्या के समाधान के लिए कार्य स्वरूप तैयार करना कृती संशोधन का मुख्य कार्य है। इस संशोधन के अंतर्गत समस्या के समाधान के लिए कृति कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक रीति से समस्या का समाधान खोजा जाता है। समाधान को व्यवहार में लाने एवं समस्या को समाधान तक पहुंचाने के लिए शोधकर्ता सतत प्रयत्नशील होता है तथा ऐसा करने से उसका शोध प्रमाणिक भी होता है।
- प्रयोगशाला संशोधन – यह संशोधन जब विज्ञान से संबंधित होता है तो प्रयोगशालाओं में किया गया शोध कार्य प्रयोगशाला संशोधन कहलाता है किंतु यह संशोधन सामाजिक स्तर पर किया जाए तो संशोधन के लिए लगने वाला विशिष्ट वातावरण निर्मित करके किसी स्थान विशेष पर सभी प्रायोगिक सुविधाओं के साथ किया गया संशोधन प्रयोगशाला संशोधन कहा जाता है। इस संशोधन में कृत्रिम उपकरणों के द्वारा निरीक्षण किया जाता है और निष्कर्ष को प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला संशोधन पूर्णतया प्रयोग रीति पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं जिनका आधार बनाकर संशोधन को गति प्राप्त होती है और संशोधन को प्रमाणिक बनाया जाता है।
- मूल्यमापन संशोधन – यह संशोधन शोध कार्य के परीक्षण की एक पढ़ती है। इस संशोधन में विषय के तथ्यों के आधार पर तथा स्थिति सापेक्ष के अनुरूप गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। किसी शोध कार्य की प्रायोगिकता के समय पर किया गया प्रशिक्षण समकालीन मूल्यमापन कहलाता है। इसी प्रकार शोध कार्य की प्रयोगिता के समय पर किसी कालखंड विशेष में किया गया गुणवत्ता परीक्षण कल नियोजित मूल्यमापन कहलाता है जिसे कालिक मूल्यमापन भी कहा जाता है। शोध कार्य के पूर्ण हो जाने पर सामाजिक एवं प्रायोगिक दृष्टिकोण से किया गया अंतिम परीक्षण सत्रान्त अथवा कार्यन्त मूल्यमापन कहलाता है। मूल्यमापन संशोधन शोध कार्य के किसी भी सत्र में किया जा सकता है। शोध कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण उसकी प्रायोगिकता के आधार पर किया जाता है प्रायोगिकता को पूर्णतः परिष्कृत रूप से परखने में मूल्यमापन संशोधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूल्यमापन के द्वारा शोध कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होती है साथ ही मूल्यमापन से शोध कार्य की उपयोगिता भी बढ़ जाती है। मूल्यमापन के द्वारा यह ज्ञात होता है कि समाज के किस क्षेत्र को प्रस्तुत शोध कार्य की कितनी आवश्यकता है। जिस की आवश्यकता अनुसार समाज के संबंधित वर्गों को शोध का लाभ प्राप्त होता है।
सामाजिकता एवं वैज्ञानिकता के अतिरिक्त शोध को कुछ अन्य आयाम के द्वारा भी समझा जा सकता है। जैसा की पूर्व में यह कहा गया है कि शोध के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। शोध को किसी निश्चित दायरे में बांधकर कार्य कर पाना कठिन होता है अतः शोध कार्य के कुछ प्रकार निर्धारित किए गए हैं जो की पूर्व में बताया जा चुके हैं किंतु शोध के कुछ आयाम भी हैं जो भाषा अथवा साहित्य की दृष्टि से समझ जा सकते हैं। शोध के असंख्य प्रकार होने पर भी शोधकर्ता एक सीमांकन के साथ शोध कार्य को करता है। जिससे कि शोध कार्य की गुणवत्ता बनी रहे। शोध के दो प्राथमिक आयाम हो सकते हैं आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ । आत्म निष्ठ शोध संसार के रहस्यात्मक तथ्यों को उद्घाटित करने का माध्यम है। जैसे कि वैदिक संहिताओं के गुण अर्थ दार्शनिक एवं आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का शमन इत्यादि। प्राचीन समय में महर्षि गूढ़ रहस्यात्मक विद्याओं में पारंगत हुआ करते थे जिससे उन्हें तत्वों का साक्षात्कार प्राप्त होता था। कहां जाता है प्राचीन समय में ज्ञान का माध्यम श्रुति परंपरा हुआ करता था, उस समय के ऋषि मंत्रों को देखने में सक्षम थे – ऋषयो मंत्रदृष्टारः।
आधुनिक काल में भी गूढ़ रहस्यों का ज्ञान रखने वाले महर्षि तुल्य संत हुए हैं जिन्होंने आत्मनिष्ठ शोध मार्ग से तत्वों का साक्षात्कार किया है इस मार्ग के ज्ञानवन्त लोगों में महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विशुद्धानंद, म.म. गोपीनाथ कविराज, म.म. मधुसूदन ओझा तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिळक इत्यादि मनीषी प्रमुख हैं।
शोध के दूसरे आयाम वस्तुनिष्ठ शोध का क्षेत्र विस्तृत माना गया है। इस आयाम के अंतर्गत मनुष्य की भौतिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण होता है। यह शोध मानविकी तथा समाजशास्त्रीय विषयों पर अवलंबित है। संस्कृत जगत का वाङ्मय भी अति विस्तृत है जो की वस्तुनिष्ठ शोध के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। संस्कृत जगत में शोध की अवसीमित संभावनाएं व्यक्त की गई है इसकी विशालता को समझ पाना अत्यंत कठिन है संस्कृत का वाङ्मय वैदिक तथा लौकिक रूपों में उपलब्ध होता है। वैदिक स्वरूप में संहिता पुराण उपनिषद इत्यादि ग्रंथ समाहित है। इसी प्रकार लौकिक स्वरूप में आदि काव्य वाल्मीकि रामायण से लेकर अनेकों महाकाव्य, गद्यकाव्य, खंडकाव्य, व्याकरण, धर्मशास्त्र, मीमांसा, संगीत, काव्यशास्त्र तथा गणित आदि विषय स्वीकार किए जाते हैं। “प्राचीन आचार्य ने विद्या स्थान के अंतर्गत उनकी गणना की है आरंभ में विद्याएं चार प्रकार की बताई गई है आण्विक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति। कालांतर में इनकी संख्या 14 बताई गई – अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या एताश्चतुर्दशा ॥ फिर इनकी संख्या में वृद्धि हुई और बढकर 18 हो गई ।” – नैषधीयचरितम् , १ /४-५ । अपि च आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं चेत्यनुक्रमात् । अर्थशास्त्रं चतुर्थं च विद्या अष्टादश स्मृताः ॥
यद्यपि शोध के आयाम अनेकों हो सकते हैं किंतु उनके सिद्धांतों का निष्कर्ष पूर्वक परीक्षण करने पर वह शास्त्र सम्मत ही सिद्ध होते हैं। शोध कार्य शास्त्र संबद्धता के कारण विस्तृत क्षेत्र को प्राप्त करता है। यदि शोध साहित्य से संबंधित है तो वह अन्य शास्त्रों से भी अवश्य ही संबंधित होगा इस आधार पर शास्त्रीय शोध के प्रकारों में वृद्धि होती है क्योंकि साहित्य की सभी विधाएं परस्पर अन्य शास्त्रों से अन्तः संबंध रखने वाली है क्योंकि विद्वान् लोगों को अनेक मार्गी कहा गया है – विद्वान्सो नैकमार्गीयः। और कवियों के विषय में कवयः क्रान्तदर्शिनः ऐसा कहा गया है। क्रांतदर्शी अर्थात काल की परिधि से बाहर जाकर भूत, भविष्य और वर्तमान को देख पाने की शक्ति रखने वाला । यहां खाने का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी प्रतिभाशक्ति के द्वारा समाज को इतिहास, वर्तमान और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का कविता के माध्यम से संकेत देकर उन्हें सचेत करते हैं। इस प्रकार कवियों का ज्ञान विविध शास्त्रों से जुड़ा हुआ होता है तथा कवियों द्वारा लिखा गया साहित्य बहुत व्यापक एवं गूढ़ अर्थ को देने वाला होता है। साहित्य के क्षेत्र में शोध विधाओं के आयामों को स्पष्ट करने के लिए वर्गीकरण रीति का सहयोग लिया जा सकता है। वर्गीकरण के द्वारा शोध के आयाम को वर्गीकृत करके शोधकर्ताओं एवं समाज के लिए सुगम मार्ग निर्माण किया जा सकता है। वर्गीकरण के माध्यम से शोध को व्यावहारिक और उपयोगी किया जा सकता है जैसे की वर्गीकरण के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं –
- ग्रंथ आधारित शोध – शोधकर्ता जब किसी पुस्तक को आधार बनाकर संशोधन कार्य करता है तो संशोधन की यह विधा ग्रंथ आधारित शोध कही जाती है। ग्रंथ आधारित शोध भी कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है किंतु इसके दो मुख्य प्रकार हो सकते हैं –
क. एक ग्रन्थीय शोध – शोधकर्ता यदि किसी एक ग्रंथ विशेष को लेकर उसके विविध तथ्यों का परीक्षण कर संशोधन पूर्ण करता है तो यह प्रकार एक ग्रंथीय शोध कहलाता है।
ख. बहुग्रंथीय शोध – जब शोधार्थी संशोधन के लिए यदि एक से अधिक ग्रंथों का उपयोग करता है तो यह शोध कार्य बहु ग्रंथीय शोध के अंतर्गत आता है। बहु ग्रंथीय शोध व्यापक विषयों वाला होता है क्योंकि इस शोध में दो अलग-अलग ग्रन्थों की समानताओं और विषमताओं का परीक्षण किया जाता है। इस शोध को तुलनात्मक शोध भी कहा जा सकता है। तुलनात्मक शोध कहने का कारण यह है की जब दो ग्रन्थों की विषमताओं और समानताओं पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया जाएगा तो उसका आधार तुलना पद्धति ही होगी। तुलनात्मकता के द्वारा ही दोनों ग के समान गुणों एवं विषम गुणों को परखा जा सकता है।
ग्रंथ आधारित शोध के उपरोक्त दोनों ही प्रकार शोध की दृष्टि से अत्यंत सरल श्रेणी में रखे जा सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्रकार के शोध कार्यों में शोधार्थी को सामग्री संकलन करने के लिए बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। शोधार्थी अपनी रुचि के अनुसार ग्रंथ का चयन कर सकता है और तुलनात्मक विमर्श के द्वारा बहु ग्रंथीय शोध भी कर सकता है। दोनों ही प्रकारों में शोधार्थी अपनी रुचि के अनुरूप बिना किसी आयस के शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए अग्रेषित हो सकता है।
विशेष विषय पर आधारित शोध – शोध का यह प्रकार प्रवृत्ति के आधार पर परखा जाता है क्योंकि शोधार्थी अपनी रुचि में प्रवृत्ति रखकर विषय का चयन करता है जो की संक्षिप्त होते हुए भी व्यापक होता है। अतः यह शोध प्रवृत्ति परख शोध भी कहा जा सकता है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है शोध के विविध आयाम हो सकते हैं उसी प्रकार शोध विषय के भी विविध प्रकार हो सकते हैं जिन्हें अलग-अलग दृष्टि से विवेचित किया जा सकता है। प्रत्येक शोधार्थी जो की प्रवृत्ति के अनुरूप विषय का चयन करता है वह ग्रंथ की किसी एक अवधारणा पर विशेष बल देकर कार्य का आरंभ करता है। और इस प्रकार के शोध के द्वारा ही ग्रंथ का विशेष स्वरुप समाज के सामने निकाल कर आता है। आज महाकवि कालिदास को उपमा अलंकार के लिए विशिष्ट स्थान प्रदान किया जाता हैं क्योंकि किसी शोधार्थी के द्वारा उपमा अलंकार पर विशेष बल देकर शोध किया गया और समाज को यह ज्ञात हुआ की महाकवि कालिदास की उपमा सर्वोत्कृष्ट है। इसी प्रकार महाकवि भवभूति के द्वारा निरूपित किया गया करुण रस तथा महाकवि भरवी का अर्थ गौरव भी समाज को प्राप्त हुआ। इस प्रकार विषय आधारित शोध के द्वारा साहित्य के क्षेत्र में एक नवीन गुण का उदय होता है जो की आने वाले शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है।
अंतर्विषय आधारित शोध – परस्पर अंतर संबंध रखने वाले विषयों को आधार बनाकर किया जाने वाला संशोधन इस प्रकार के शोध के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। इस शोध में प्रति होने वाला शोधार्थी दो अथवा दो से अधिक ग्रन्थों को प्रौढ़ रूप से जानने वाला होता है। शोध के इस प्रकार में मूल विषय से संबद्ध अन्य ग का चयन किया जाता है तथा उन पर विशेष अध्ययन करना होता है। कालिदास के ग्रन्थों में औषधीय गुणों वाली वनस्पतियों का उल्लेख अथवा मम्मट विरचित काव्य प्रकाश में काश्मीर दर्शन का उल्लेख इस प्रकार के शोध विषय इसी श्रेणी में आते हैं। इस शोध प्रकार के द्वारा चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्यकला, पर्यावरण तथा प्राचीन भौगोलिक स्थिति इत्यादि ऐतिहासिक मूल्यांकन के क्षेत्रों का ज्ञान समाज को होता है।
समस्या के आधार पर शोध – किसी भी शोध कार्य का आरंभ जिज्ञासा अथवा समस्या के कारण ही होता है। समस्या अथवा जिज्ञासा के अभाव में शोध कार्य अपने चरम को प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि जब तक शोधार्थी जिज्ञासा के कारण समस्या का समाधान करने के लिए प्रति नहीं होगा तब तक शोध के द्वारा नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। शोध की मूल अवस्था समस्या हो सकती है जिसे दो भागों में विभाजित कर शोध किस मार्ग पर किया जाए इसका निर्णय किया जा सकता है। समस्याएं दो प्रकार की कहने का तात्पर्य यह है की पहली समस्या वह है जिसमें अनंत्य दोष होता है। जैसे की बीज और वृक्ष में पहले किसकी उत्पत्ति हुई इस समस्या को अनंत्य समस्या कहा जाता है। ऐसी समस्या के आधार पर शोध नहीं करना चाहिए क्योंकि इस शोध का कोई कल निश्चित नहीं है और ना ही इस से समाज को कोई लाभ होने वाला है। समस्या का दूसरा प्रकार वह है जिसका समाधान संभव है और उसे संभव समाधान से समाज को लाभान्वित करना शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य है। एक शोधार्थी को ऐसी ही समाधान की संभावना वाली समस्या पर शोध करके समाज को लाभान्वित करना चाहिए। आज संस्कृत के क्षेत्र में वैदिक और पौराणिक वाङ्मय में समाधान वाली समस्याओं के शोध विषय भरे पड़े हैं जिन पर शोध की बहुत आवश्यकता है। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है और भारत की संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति के नाम से विश्व विख्यात है आज है इस वैज्ञानिक संस्कृति के मूल ग्रन्थों में विज्ञान की खोज करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। इसी प्रकार संस्कृत के साहित्य में भी अनेकों समस्याएं हैं जिनका समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है उदाहरण के लिए संसार महाकवि कालिदास की रचनाओं का हृदय से आनंद लेता है लेकिन उन्हें महाकवि का प्रमाणिक परिचय किसी भी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। सभी इतिहासकार एवं काव्य मर्मज्ञ परस्पर विरोधी मतों में उलझे हुए हैं मतों के विरोध को सुलझाकर किसी सिद्धांत का प्रतिपादित करने या समाज को प्रमाणित ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता है ना कि विरोध में उलझे रहने की।
क्षेत्र के आधार पर शोध – स्थान और समय को सीमित करके साहित्य, इतिहास अथवा अन्य किसी विषय में किया जाने वाला शोध कार्य इस श्रेणी में आता है। समय और क्षेत्र की सीमाओं के कारण यह शोध अन्य विषयों का स्पर्श नहीं करता है जिससे कि एक निश्चित जानकारी ही प्राप्त हो पाती है। कश्मीर की शैव परंपरा, उत्तर भारत अथवा दक्षिण भारत की स्थापत्य कला, भारत के किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां, एशिया महाद्वीप की दंत कथाओं में रामायण का वर्णन, 21वीं शताब्दी के महाकाव्य अथवा नाटक तथा भारत के प्रमुख तीर्थ क्षेत्र इत्यादि इस संशोधन के उदाहरण हैं। प्रायः ये विषय सीमित प्रतीत होते हैं किंतु उनके द्वारा विभिन्न कॉल करो के साहित्य एवं उसे समय विशेष की संस्कृति का अपार ज्ञान भंडार प्राप्त होता है। तथा उनके द्वारा आगामी शोध की प्रचुर संभावनाएं विद्यार्थियों को प्राप्त होती है जो की उन्हें शोध के लिए प्रेरित करती है।
- पांडुलिपि आधारित शोध – पांडुलिपि अर्थात प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथ। पांडुलिपियों का संपादन करना और पांडुलिपियों मैं निहित विषयों का संशोधन करना दोनों भिन्न-भिन्न कार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में पांडुलिपि संपादन को शोध के अंतर्गत रखा गया है लेकिन यह शोध कार्य का अंग मात्र है। पांडुलिपियों का व्यवस्थित एवं दोष रहित संपादन करना शोध कार्य का एक भाग है। इसके द्वारा शोध कार्य में नवीन तथ्यों का संकलन कर समाज को प्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथ के मूल विषय से अवगत करवा कर उससे होने वाले लाभ की जानकारी दी जा सकती है।
पांडुलिपि संशोधन के क्षेत्र में प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र तथा डॉ. गोविंद गंधे इन दोनों विद्वानों ने अपनी – अपनी पुस्तकों में पांडुलिपिशोध के प्रकारों को इस प्रकार बतलाया है –
(१) अवलोकन अनुसन्धान – अवलोकन का तात्पर्य है वास्तविकता, तथ्य व व्याख्या को संग्रहीत करके उसको लिखना अथवा उन्हें परोक्ष सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में तथा बड़े व्यापक क्षत्र में प्रयुक्त किया गया है, जिससे अवलोकन कर्ताओं को सामाजिक क्रियाकलापों में सम्मिलित होना पड़ता है और उसके आस- पास होने वाली क्रियाओं को देखना पड़ता है। अवलोकन अनुसन्धान के लिए अवलोकन सर्वे प्रयोग में लिखा जाता है। खगोल विज्ञान में बहुत से तथ्य अवलोकन के द्वारा ही ज्ञात किये जाते हैं। यह अनुसन्धान के प्रथम चरण का निर्माण करता है।
(२) आनुभविक अनुसन्धान – इस अनुसन्धान के अन्तर्गत अवलोकन के परिणामों को सङ्कलित करके वर्गीकृत किया जाता है और उनके आधार पर सांख्यिकी विधि से निष्कर्ष निकाल कर साधारण समीकरण, सह-सम्बन्ध तथा निश्चित तथ्यों के सामान्यीकरण सम्बन्धों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें पूर्वानुपाती आयाम कहते हैं। जिस मानसिक प्रक्रिया के आधार पर नियमों को निकालते हैं, उन्हें अनुमान कहा जाता है। अनुमान के लिए आवश्यकतानुसार बुद्धि की अपेक्षा होती है। इसे आनुभविक अनुसन्धान की संज्ञा दी जाती है। यह अनुसन्धान वास्तविक अनुसन्धान है।
(३) मौलिक अनुसन्धान – आनुमानिक नियमों के विपरीत मौलिक नियम बिना किसी बौद्धिक साधना के प्राप्त किये जा सकते हैं। वास्तव में इनमें आन्तरिक ज्ञान का अत्यधिक प्रभाव होता है। आन्तरिक ज्ञान द्वारा बिना किसी बुद्धि व्यायाम के, चेतना, बुद्धि, प्रत्यक्ष आदि वस्तुओं की जानकारी स्वतः ही हो जाती है। एक मनुष्य, जिसे यह ज्ञान हो जाता है, उसे सिद्ध या सन्तमहात्मा कहते हैं।
(४) पूर्व अनुसन्धान – इसके अन्तर्गत हम जिस प्रक्रिया में कार्य करते हैं, वह अनुमान है। अनुसन्धान के अन्तर्गत बुद्धि की एक मुख्य भूमिका होती है। इसके दो भाग होते हैं- (१) विशुद्ध अनुसन्धान, (२) अनुप्रयुक्त अनुसन्धान।
(५) विकासात्मक अनुसन्धान – विकासात्मक अनुसन्धान वह शब्द है जो या तो पूर्वगामी अनुसन्धान है या प्रयोगवादी अनुसन्धान से उत्पन्न होता है, तथा यह पूर्व प्राप्त परिणाम जो आवश्यक एवं तत्कालीन उपयोगिता को प्राप्त करने के लिये किये जाते हैं, वे आवश्यकता तथा तत्कालीन उपयोगिता के मध्य सम्बन्धों में सुधार लाते है। इस अनुसन्धान की आवश्यकता सभी उद्योगों में जानी जाती है तथा कई उद्योगों के पार्श्व में इस विकासात्मक अनुसन्धान को देखा जा सकता है।”