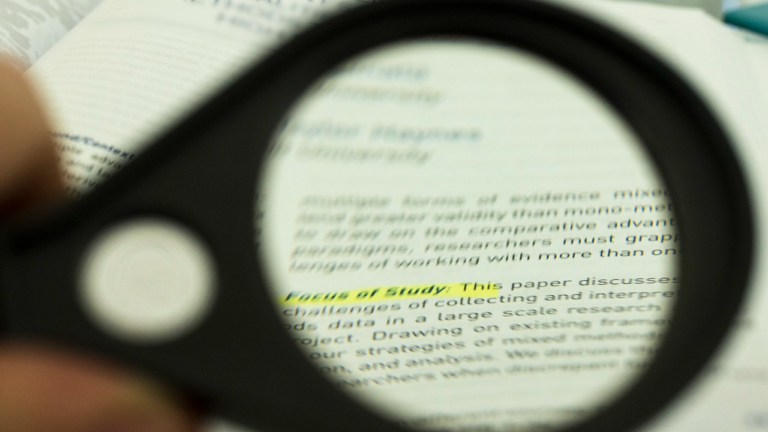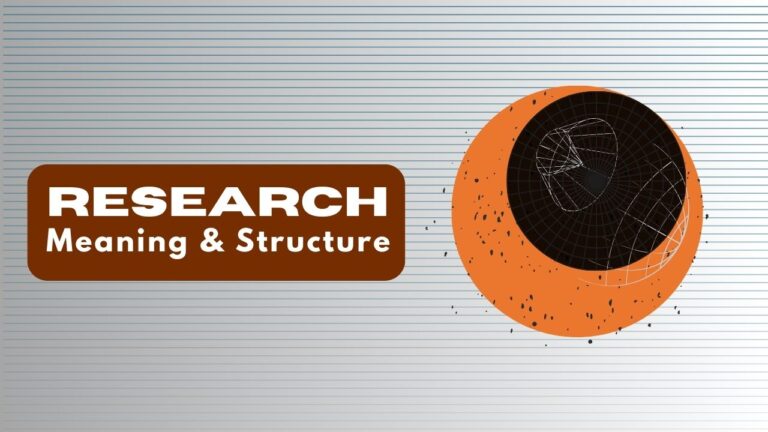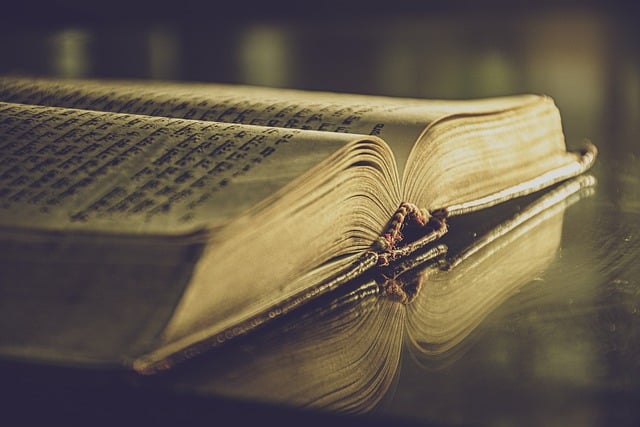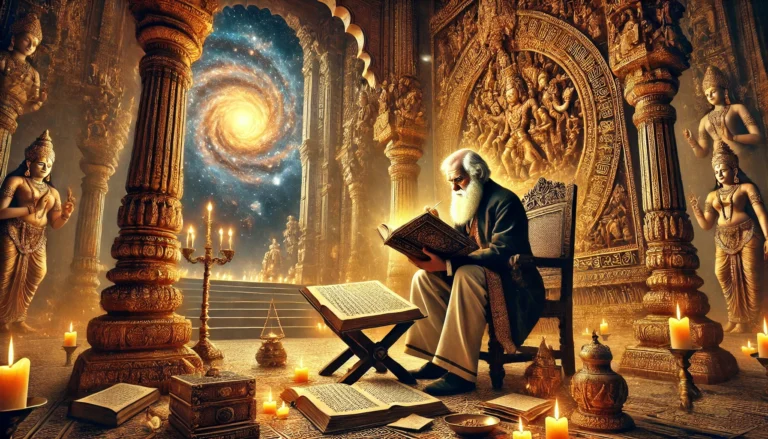Sanskrit language and literature संस्कृतभाषा व साहित्य
संस्कृतभाषा प्राचीन काल से ही भारतीय शास्त्रपरम्परा की वाहिनी रही है । प्राचीन भारतीय ग्रन्थ संस्कृत के आश्रय से ही समृद्ध हुए हैं । भारतीय वेद. वेदांग, दर्शन, कला आदि समस्त साहित्यग्रन्थों को संस्कृत ने ही अपने अंक में स्थान दिया है । संस्कृतभाषा समस्त भारतीय भाषाओं में अग्रगण्य तथा जननी स्वरुपा है । अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं में भी अधिकांश भाषाएं संस्कृत भाषा से प्रभावित है । संसार के सभी भाषा वैज्ञानिक संस्कृत को उत्कृष्टतमा एवं वैज्ञानिक भाषा का पद प्रदान करते है । संस्कृत भाषा में प्राप्त साहित्य अनन्त था किन्तु कालान्तर में हमें उस साहित्य महासागर के कुछ बिन्दु ही प्राप्त हुए हैं । तथापि उपलब्ध संस्कृत के ग्रन्थ साहित्यविद्या, भाषा, विज्ञान तथा अन्य तकनीकि क्षेत्रों में अपूर्व योगदान प्रदान करते है । आज समस्त संसार संस्कृत के गूढ रहस्यों को जानने के लिए तत्पर है ।
वर्तमान काल में संस्कृत भाषा में प्राप्त साहित्य पर बहु आयामी संशोधन किया जा रहा है । नाना विध क्षेत्रों में संस्कृत का वाङ्मय अपनी प्रतिभा को प्रकाशित कर रहा है । संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है बल्कि एक युग सेतु है जो अनादि काल से चली आ रही परम्पराओं और ज्ञान-विज्ञान की धाराओं को अपने माध्यम से एक युग से दुसरे युग तक पहुचाता आया है । प्राचीन संस्कृत वाङ्मय आज सामित संख्या में उपलब्ध है किन्तु संस्कृत का ज्ञान भंडार असीमित है । अनेकों वर्षों के उपरान्त भी संस्कृत का अमृतत्व यथावत् बना हुआ है । ऐसी अमृतवाणी का साहित्य भी अमृतत्व देने वाला ही है ।
संस्कृत निष्ठ साहित्य का अनेकों प्रकारों से शोध किया जा सकता है । संस्कृत में प्राप्त वाङ्मय में वेद, वेदांग, दर्शन, साहित्य, भाषा, वास्तु, खगोल, रसायन, तकनीकि तथा चिकित्सा जैसे अनेकों विषयों का उल्लेख प्राप्त होता है । आज सम्पूर्ण विश्व में जो भी शोध का विषय है उस शोध का आधार कहीं ना कहीं संस्कृत में प्राप्त उल्लेख ही है । विश्व के प्रत्येक संशोधन केन्द्र (रिसर्च सेंटर) में और कुछ हो या ना हो किन्तु वेद, पुराण, उपनिषद्, रामायण तथा महाभारत अवश्य प्राप्त होते हैं । क्योंकि संसार के सभी वैज्ञानिक और गवेषक जानते हैं कि अगर किसी समस्या का समाधान बाहर नहीं मिल रहा है तो संस्कृत वाङ्मय में अवश्य मिलेगा ।
संस्कृत जगत् में अनेकों कवि हुए हैं । उनके साहित्य का संकल्पनात्मक विस्तार असीमित है । फिर भी कालखण्ड के आधार पर उन कवियों को और काव्य रचनाओं को एक सूत्र में लाने के लिए समकालिनता के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है –
समकालीन संस्कृत साहित्य –
समकालीन अर्थात समान काल, ऐसे साहित्य ग्रन्थ जिनका रचना काल समान हो उन्हे समकालीन कहा जाता है । इस कालखण्ड को एक परिधि के द्वारा भी समझा जा सकता है । यथा – 5वीं शताब्दी के साहित्य ग्रन्थ अथवा 6ठी शताब्दी के ग्रन्थ ।
संस्कृत भाषा में प्राप्त वेद अपौरुषेय है अत- उनका काल निर्णय करना असम्भव है तथापि कुछ पाश्चात्य विद्वान् अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार वेदों का काल निर्णय करने का प्रयास करते है ।
मेक्समूलर के अनुसार वेदों का रचना काल 1200 से 2500 ई.पू. है ।
जेकौबी के अनुसार वेदों का काल 3000 से 4000 ई.पू. है ।
लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष के आधार पर वेदों का रचना काल 6000 ई.पू. होने का अनुमान प्रकट किया है ।
काव्यशास्त्र तथा काव्यग्रन्थों के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो काल निर्णय कुछ इस प्रकार से होगा –
आर्षकाव्य रामायण –
महर्षि वाल्मीकि विरचित यह महाकाव्य भारतीय संस्कृति की नीव का पत्थर है । इस 24000 पद्यो वाले महाकाव्य ने भारतीय जन मानस में अपनी अद्वितीय छवि को अंकित किया है । यह महाकाव्य साक्षात् ईश्वर स्वरुप कहा जा सकता है । आधुनिक युग में जर्मन् के विद्वान् श्लेगल इस महाकाव्य का रचना काल 1100 ई. पू. मानते है । रामायण के काल को सुस्पष्ट लिख पाना किसी भी तत्त्ववेत्ता की ज्ञान सीमा से बाहर है । प्राचीन अथवा अर्वाचीन भारतीय अथवा पाश्चात् सभी सुधीजन मात्र अनुमान ही कर सकते है । इसी अनुमान की शृङ्खला में याकोबी 800 ई.पू. से 500 ई.पू., कामिल बुल्के 600 ई.पू. रामायण का रचना काल अनुमानित करते है ।
मैकडोनल, काशीप्रसाद जायसवाल तथा जयचन्द्र विद्यालंकार इस महाकाव्य को 500 ई.पू. में विरचित मानते है । (Macdonell – A history of Sanskrit literature, p. 306-309) इस ग्रन्थ में भारत की 500 ई.पू. वर्ष पुरानी संस्कृति का चित्रण प्राप्त होता है अतः कुछ विद्वान् इसा प्रामाणिक समय 500 ई.पू. मानने का दावा करते है (संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, पृ.108) किन्तु यह भी सम्भव है कि सनातन संसिकृति में आरम्भ से लेकर 500 ई.पू. तक अधिक परिवर्तन नही पुए हो । अतः उन परिवर्तनों को परख पाना सम्भव नहीं हुआ हो । भारत में रामायण उपाधि वाले अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते है जिनमें भगवान् राम की कथा का वर्णन है – योगवासिष्ठ( वसिष्ठ रामायण), आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण इत्यादि ।
महाभारत –
महर्षि कृष्णद्वेपायन वेदव्यास द्वारा रचा गया भारत का ऐतिहासिक महाकाव्य जिसमें भारत वर्ष में की गई धर्मस्थापना की गाथा उल्लिखित है, महाभारत के नाम से समूचे विश्व में विख्यात है । इस महाकाव्य की गाथा भारत तथा समीपवर्ती प्रत्येक देश में बुजुर्गों द्वारा अपनी नई पीढी को सुनाई जाती है । इस महाकाव्य में 1 लाख श्लोकों का संग्रह है जो द्वापर युग की नीतियों और धर्मस्थापना की गाथाओं का व्याख्यान करता है । महाभारत के विषय में कहा जाता है – यन्न भारते तन्न भारते । अर्थात् जिसका उल्लेख महाभारत में नहीं है वह भारत में नहीं है । महाभारत के तीन विभाग माने जाते है । ऐसा कहा जाता है कि महाभारत की रचना तीन भागों में हुई है – जय, भारत और महाभारत ।
जय संहिता –
महाभारत का जय नामक भाग मूल भाग तथा महाभारच का आरम्भिक भाग माना जाता है । महाभारत के मंगलाचरण में भी जय का ही उल्लेख प्राप्त होता है – नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् । अर्थात् नारायण को, नरों में उत्तम नर अर्जुन को, देवी सरस्वती को और महर्षि व्यास को नमस्कार करके जय नामक ग्रन्थ को पढा जाना चाहिए । इस जय नामक संहिता में श्लोक संख्या को निर्दिष्ट करने वाला एक पद्य है –
अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च ।
अहं वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वा ।। ( आदिपर्व, 1/81)
इस श्लोक में 8800 श्लोकों का उल्लेख है तथा व्यास के शिष्यों (जैमिनि, पैल, वैशम्पायन,सुमन्तु तथा शुक)में से शुक उल्लेख है । ऐसा माना जाता है कि व्यास के पाचों शिष्यों ने जय संहिता के पृथक्-पृथक् संस्करण किये थे किन्तु जैमिनि के अश्वमेध पर्व तथा वैशम्पायान की भरत संहिता को छोडकर सभी संस्करण नष्ट हो गए हैं ।
भारत संहिता –
जय संहिता का विस्तार रुप भारत संहित के रुप में उदित हुआ है । यह महाभारत की द्वितीय अवस्था है । यह 24000 श्लोकों का विशाल महाकाव्य है । महाभारत के आदि पर्व में इस उपाख्यान रहित संहिता के विस्तार का उल्लेख प्राप्त होता है –
चतुर्विंशतिसहस्रीं चक्रे भारतसंहिताम् ।
उपाख्यानैर्विना तावद् भारतं प्रोच्यते बुधैः ।। (आदिपर्व, 1/102-103)
महाभारत संहिता –
यह महाभारत की अन्तिम अवस्था है । यहीं संहिता आज हमें उपलब्ध होती है । इस स्वरुप में 1 लाख श्लोकों का महासागर है जिसमें भारत के द्वापर युग का तथा धर्मस्थापना का विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया है ।
इस ग्रन्थ का काल निर्णय करना अत्यन्त कठिन है । वेदावयव गृह्यसूत्रादि में इसका उल्लेख प्राप्त होता है । अनेकों प्राचीन कवियों ने भी अपने – अपने काव्यों के लिए महाभारत को आधार बनाया है तथा काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में महाभारत के पद्यों का उदाहरण देकर इसका उत्कृष्टता को सिद्ध किया है । महाभारत का उल्लेख केवल भारतीय शास्त्रों में ही प्राप्त नही होता अपितु यूनानादि देश के विद्वान् भी इसका उल्लेख करते है । इस महागाथा का उल्लेख 50 ई. में यूनान के दियो क्रिसोस्तोम ने इलियड नाम से, 5वी. शताब्दी के दानपात्रों पर धर्मशास्त्र के नाम से, 6ठी शताब्दी के सुबन्धु और 7वी शताब्दी के बाणभट्ट के द्वारा, 8वी शताब्दी के कुमारिलभट्ट के द्वारा, 11वी शताब्दी के कश्मीरी करवि क्षेमेन्द्र के द्वारा तथा कालन्तर में भासादि नाटककारों के द्वारा विविध रुप में महाभारत का उल्लेख किया है । महाभारत का उल्लेखआश्वलायन गृह्यसूत्र में तथा बौधायन गृह्यसूत्र में प्राप्त होता है । बौधायन गृह्यसूत्रों का काल 400 ई.पू. माना गया है । अतः महाभारत की जय संहिता को 800 ई.पू., भारत को 500 ई. पू. तथा महाभारत को 200 या 100 ई.पू. के लगभग मना जा सकता है ।
पुराण साहित्य –
प्राचीन भारतीय साहित्य में पुराण साहित्य भी ऐतिहासिक साहित्य के अन्तर्गत परिगणित किये गए हैं । महाभारत कि एक उक्ति है – इतिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपबृंहयेत् । अर्थात् वेद के अर्थ का व्याख्यान इतिहास और पुराण ग्रन्थों के द्वारा किया जाना चाहिए । पुराणों में वैदिक ज्ञान को रोचक गाथाओं के माध्यम से तथा तत्कालीन राजाओं के कथानकों के द्वारा जन समान्य को समझाने का प्रयत्न किया गया है । व्यास विरचित अष्टादश पुराण भारतीय इतिहास की धरोहर हैं । इनमें 10 पुराण शिव से,4 पुराण ब्रह्मा से 2 पुराण देवी से तथा 2 पुराण हरि से सम्बद्ध है –
अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः ।
चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हरिः ।। (स्कन्दपुराण, केदारखण्ड,1)
पुराणों के रचनाकाल के विषय में साहित्यजगत् में अनन्त वैमत्य है तथापि कुछ मत है जो अनुमान के तर्क के निकटवर्ती कहे जा सकते है ।
बालगंगाधर तिलक के अनुसार पुराणों का रचना का उत्तरवर्ती काल 2री शताब्दी है । (गीतारहस्य, पृ.566)
पार्जिटर ने पुराणों में राजनीतिक इतिहास का अध्ययन किया और पाया कि पुराण 1ली शताब्दी में ही अपने अस्तित्व को प्राप्त कर चुके थे ।
डॉ. आर. सी हाजरा के मत में पुराणों की रचना 100 वर्षों का परिश्रम नहीं है । उन्होने अलग-अलग पुराणों का रचना काल अलग-अलग कालखण्ड को माना है । उनके अनुसार पुराण 2री – 3री शताब्दी से 10वी शताब्दी तक लिखे जाते रहे । (R.C. Hazra – Puranic Records on Hindu Rights And Customs, 1940)
काव्यविधाए एवं उनके कवि –
संस्कृत साहित्य जगत् में काव्य को दो प्रकार से विभाजित किया गया है – दृश्य और श्रव्य । दृश्य काव्य नाटक के रुप में प्रसिद्ध है तथा श्रव्य काव्य के तीन प्रकार माने गए हैं – गद्य पद्य और चम्पू ।
गद्यकाव्य, कथा और आख्यायिका के रुप में और पद्यकाव्य, महाकाव्य और खण्डकाव्य के रुप में प्रचलित हुए । पुराण काल से परवर्ती कवियों ने अनेक प्रकार के काव्य और लक्षणग्रन्थों की रचना की है । कुछ कवि पुराण काल के कवि भी रहे है जिन्होनें पुराणों के उद्धरण अपने काव्यों में दिए हैं । सम्प्रति कालक्रमानुसार कवियों एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है –
प्रथमशताब्दी के कवि –
कालिदास –
संस्कृत साहित्य की बात हो तो महाकवि कालिदास की गणना सर्वप्रथम होती है । इसीलिए कालिदास को कनिष्ठिकाधिष्ठित कहा गया है । – पुराकवीनां गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः । अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव।।
कालिदास उत्तम कवि तथा श्रेष्ठ नाटककार हैं । महाकवि का अभिज्ञानशाकुन्तलं नाट्यजगत् का कीरीट है । इस रचना की ख्याति में कहा गया है – काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला । महाकवि कालिदास की सात रचनाएं प्राप्त होती हैं जो महाकाव्य, खण्डकाव्य तथा नाटक के रुप में हैं ।
महाकाव्य – रघुवंशम् व कुमारसम्भवम्
खण्डकाव्य – ऋतुसंहार व मेघदूतम्
नाटक – मालविकाग्निमित्रम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् व विक्रमोर्वशीयम् ।
कालिदास के काल के विषय में इतिहास में पर्याप्य वैमत्य प्राप्त होता है । इतिहासकार कालिदास को प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी तक मानते है किन्तु महाकवि के प्रमाण प्रथमशताब्दी से पूर्व के भी प्राप्त होते है । इतिहासकार कालिदास को ईसा से एक शताब्दी पूर्व मानते हैं । अतः कालिदास का समय प्रथम शताब्दी से कुछ पूर्व का ही स्वीकार किया गया है ।
अश्वघोष –
संस्कृत साहित्य में अश्वघोष का नाम कवि के अतिरिक्त धर्म के प्रचारक दार्शनिक तथा विद्वत्श्रेणी में प्राप्त होता है । अश्वघोष का नाम बौद्धभक्षु तथा आचार्य के रुप में भी प्राप्त होता है । बौद्ध साहित्य में अश्वघोष का नाम सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाता है । अश्वघोष के नाम से साहित्य में अनेकों रचनाए प्राप्त होती है । जिनमें काव्य, दर्शन तथा धर्मप्रचारक ग्रन्थ सम्मिलित हैं । इनमें प्रमाण द्वारा सिद्ध 4 रचनाएं सुप्रसिद्ध हैं – बुद्धचरित (28 सर्गों का महाकाव्य), सौन्दरानन्द (18 सर्गों का संस्कृत महाकाव्य), शारिपुत्रप्रकरण ( 9 अंकों का रुपक) तथा राष्ट्रपालनाटक (चीनी भाषा में उपलब्ध गेय नाटक) ।
अश्वघोष की प्रक्षिप्त रचनाओं को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है – प्रथम वर्ग, संस्कृत में प्राप्त रचनाएं जिनका चीनी अथवा तिब्बती भाषा में अनुवाद प्राप्त होता है या संकेत प्राप्त होते है । द्वितीय वर्ग, तिब्बती चीनी अथवा दोनों भाषाओं में केवल अनुवाद रुप में ग्रन्थ प्राप्त होते हैं ।
प्रथम वर्ग में वज्रसूची, गण्डीस्तोत्रगाथा, नैरात्म्यपरिपृच्छा, त्रिदण्डमाला तथा शतपञ्चाशत्कस्तोत्र प्रमुख हैं।
द्वितीय वर्ग में 16 ग्रन्थ हैं जिनमें महायानश्रद्धोत्पादशास्त्र तथा सूत्रालंकारशास्त्र प्रमुख हैं किन्तु विद्वानों का यह भी मानना है कि ये रचनाएं अश्वघोष की नहीं हैं ।
षष्ठी शताब्दी के कवि –
भट्टिकवि –
भट्टिकवि का काल छठी शताब्दी का उत्तरार्ध अर्थात् 550 ई. से 610 ई. स्वीकार किया जाता है । भट्टिकवि संस्कृत जगत् के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके काव्य को भी भट्टिकाव्य के नाम से ही जाना जाता है । इनके काव्य को व्याकरण और अलंकार का महासागर कहा जा सकता है । भट्टिकवि ने अपने रावणवधं (भट्टिकाव्य) काव्य की प्रशंसा में एक पद्य लिखा है –
व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुधियामलम् ।
हता दुर्मेधसश्चास्मिन् विद्वत्प्रियतया मया ।। (भट्टिकाव्य-22/34)
अर्थात् यह काव्य व्याख्या के उपरान्त ही समझा जा सकता है, बुद्धिमान लोग इसको पढकर आनन्द का अनुभव करते है किन्तु मुर्खों को तो साक्षात् मृत्यु प्राप्त हो जाती है ।
इस काव्य के लिए भामह ने भी इसी बात को उदासीनता के साथ प्रस्तुत किया है –
काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत् ।
उत्सवः सुधियामेव हन्त दुर्मेधसो हताः ।। (काव्यालंकार – 2/20)
भामह का काल भी छठी शताब्दी माना गया है । समकालीन होने के कारण सम्भवतः भट्टिकवि और भामह परस्पर परिचित रहे होंगे ।
स्वरुप की दृष्टि से इस काव्य को चार काण्डों में विभक्त किया गया है – प्रकीर्ण, अधिकार, प्रसन्न और तिङन्त । भट्टिकाव्य का महत्व शास्त्रवत् स्वीकार किया गया है –
अष्टाध्यायी जगन्माताऽमरकोशो जगत्पिता ।
भट्टिकाव्यं गणेशश्च त्रयीयं सुखदास्तु वः ।।
जगन्माता पार्वती और जगत्पिता शिव के समन्वित स्वरुप गणेश है उसी प्रकार अष्टाध्यायी और अमरकोश का समन्वित स्वरुप भट्टिकाव्य है । संस्कृत का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए इन तीनों का समन्वित स्वरुप हमारे लिए सुखप्रद हो ।
तथा निर्णयसागर प्रेस के संस्करण में बी प्रशंसा प्राप्त होती है –
व्याकृत्या कोश-छन्दोभ्यामलंकृत्या रसेन च ।
पञ्चकेनान्वितं काव्यं भट्टिकाव्यं विराजते ।।
अर्थात् व्याकरण, कोश, छन्द, अलंकार और रस इन पांच तत्वों से भट्टिकाव्य परिपूर्ण है सुशोभित है ।
भारवि –
संस्कृत साहित्य में भारवि कवि अर्थगौरव के लिए सुप्रसिद्ध है । भारवि कलापक्ष के समर्थक और विशिष्ट रचनाओं के निर्माता है । कवि भारवि का किरातार्जुनीयम् सुप्रसिद्ध है । इस महाकाव्य में पाण्डित्य प्रकर्ष के साथ-साथ कलात्मका का उत्कर्ष भी समाहित है ।
अष्टाध्यायी की वृत्ति काशिका तथा कृष्णमाचार्य की पुस्तक द हिस्ट्री में प्राप्त उद्धरणों के अनुसार भारवि का काल 550 ई. से 620 ई. माना जाता है ।
भारवि के विषय में कतिपय उक्तियां साहित्य क्षेत्र में प्रचलित है – भारवेरर्थगौरवम्, भारवेरिव भारवेः, प्रकृतिमधुरा भारविगिरः, नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवेः इत्यादि । इन उक्तियों में भारवि के रचना कौशल की शैली की स्वाभाविक मधुरता, बाह्यरूक्षता, अन्तः सरसता तथा अर्थगत गौरव इस प्रकार के वैशिष्ट्यों को प्रदर्शित किया गया है ।
सातवी शताब्दी के कवि
कुमारदास –
कवि कुमारदास अपने जानकीहरण महाकाव्य के लिए लोकप्रिय है । इनके स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद प्राप्त होते है । अनेकों प्रमाण इन्हें सिंहल देश (लंका) का निवासी सिद्ध करते हैं । इसका एक कारण यह भी है कि उनका काव्य सिंहली भाषा में यथावत् शब्दशः अनुवाद के रुप में सुरक्षित है तथा इसकी प्रतियां भी सिंहल से ही प्राप्त हुई है । वामन की प्रयोग टिप्पणी के अनुसार तथा कीथ ने काशिका का प्रभाव स्पष्ट करते हुए कुमारदास के काल को भी अनायास ही संकेतित किया है । अतः कुमार दास का काल 620 ई. के आसपास अथवा 650 ई. से 700 ई. माना जा सकता है । जानकीहरण की प्राप्त पाण्डुलिपियों में विषय मतभेद के कारण निश्चित कालखण्ड बता पाना कठिन है ।
माघ –
महाकवि माघ संस्कृत साहित्य की गरीमा को उत्कर्ष प्रदान करने वाले कवि कहे गए है । माघ का शिशुपालवधम् महाकाव्य संस्कृत साहित्य जगत् का श्रेष्ठ काव्य है । इसीलिए कहा भी गया है – काव्येषु माघः। भारवि के विचित्र मार्ग को माघ ने उत्कर्ष प्रदान किया है तथा भारवि से भी आगे बढकर विचित्र मार्ग को सफलता के शिखर तक पहुंचाया है ।
माघ श्रीमाल अथवा भिन्नमाल के निवासी माने जाते है । यह स्थान राजस्थान के माउण्ट आबू के समीप जोधपुर मण्डल में है ।
माघ ने शिशुपालवधम् के अन्त में वंश वर्णन में कुछ संकेत दिये है । जिनमें उनके पितामह का उल्लेख है । जिनके उद्धरण के अनुसार कुछ शिलालेख प्राप्त हुए है । शिलालेख में 682 सम्वत् का उल्लेख प्राप्त होता है –
द्विरशीत्यधिके काले षण्णां वर्षशतोत्तरे ।
जगन्मातुरिदं स्थानं स्थापितं गोष्ठिपुंगवैः ।। (वसन्तगढ लेख, श्लोक-11)
यह शिलालेख विक्रमसम्वत् का मानकर 625ई. समय माना जा सकता है और माघ तीसरी पीढी होने के कारण उनको 675 ई. में स्वीकार किया जा सकता है । अनेकों विद्वान् 700 ई. के आसपास ही माघ को स्वीकार करते हैं । इस प्रकार माघ का समय 650 ई. से 700 ई. के मध्य माना जा सकता है ।
कविमाघ की ख्याति विविध रुपों में विख्यात है –
उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम् ।
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ।।
अर्थात् कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, भारवि अर्थगौरव के लिए भारवि प्रसिद्ध है, दण्डि पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है किन्तु माघ ऐसे कवि है जिनके काव्य में तीनों गुण प्राप्त होते हैं ।
मध्यकाल के कवि (800 ई. से 1150 ई.)
शिवस्वामी –
कवि शिवस्वामी कश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा के राजकवि थे । ये शैवमतावलम्बी थे किन्तु चन्द्रमित्र नामक एक बौद्ध आचार्य की प्रेरणा से बौद्ध साहित्य में अनुपम योगदान प्रदान किया । इन्होने एक बौद्ध नीतिग्रन्थ कप्फिणाभ्युदय महाकाव्य की रचना की । आचार्य मम्मट ने अपने काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ में इसके एक पद्य का ध्वनि काव्य के सन्दर्भ में उदाहरणार्थ उल्लेख किया है।
काश्मीर नरेश के कालखण्डानुसार इनका काल 800 ई. से 850 ई.माना गया है ।
कल्हण की राजतरङ्गिणी में जनश्रुतियों के आधार पर एक उल्लेख प्राप्त होता है जिसमें राजा अवन्तिवर्मा के काल में मुक्ताकण, शिवस्वामी, आनन्दवर्धन तथा रत्नाकर कवियों की विशेष ख्याति का उल्लेख है –
मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः ।
प्रथां रत्नाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ।।
रत्नाकर –
राजा अवन्तिवर्मा के राज्य में रत्नाकर को भी शिवस्वामी के समान ही ख्याति प्राप्ति थी । ये चिप्पट जयापीड के शासन काल में भी आश्रित कवि रहे है । इनके ग्रन्थ में उनका उल्लेख अनेक स्थानो पर प्राप्त होता है । इस राजा को बालबृहस्पति की उपाधि प्राप्त थी । जिसका निर्देश हरविजय में प्राप्त होता है । कवि रत्नाकर को भी दो उपाधियां प्राप्त थी – राजानक और वागीश्वर । रत्नाकर की तीन कृतियां उपलब्ध होती हैं – हरविजय, वक्रोक्तिपञ्चाशिका तथा ध्वनिगाथापञ्चाशिका ।
इनका समय 800 ई. से 850 ई. माना गया है ।
अभिनन्द –
अभिनन्द नामक कवि के नाम से रचित दो भिन्न काव्य प्राप्त हुए है – रामचरित तथा कादम्बरीकथासार । इन ग्रन्थों में प्राप्त उल्लेख के अनुसार रामचरित के रचनाकार कवि स्वयं को शतानन्द का पुत्र बतलाते है और दुसरे अभिनन्द के पिता प्रख्यात नैयायिक जयन्तभट्ट हैं । इनके प्रपितामह शक्तिस्वामी गौडदेश से काश्मीर क्षेत्र में आकर बस गए थे । शक्तिस्वामी काश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीड के मन्त्री थे । रामचरित के रचयिता का सम्बन्ध भी गौडप्रदेश से रहा है अतः इतिहासकारों को दोनो की अभिन्नता का भ्रम होता है । अभिनन्द कवि के नाम से साहित्य में रामचरित, कादम्बरीकथासार तथा योगवासिष्ठसार ये तीन ग्रन्थ प्राप्त होते हैं ।
रामचित महाकाव्य के रचयिता अभिनन्द के आश्रयदाता हारवर्ष युवराज थे इतिहासकारों के अनुमान से देवपाल ही हारवर्ष माने गये है । अतः इनका काल 850 ई. के आसपास माना गया है।
क्षेमेन्द्र –
कश्मीरी कवियों में क्षेमेन्द्र कश्मीरी रत्न कहे जाते थे । ये अनेकों विषयों में रचना करने वाले कवि हैं । इनका एक अन्य नाम व्यासदास भी है । अभिनवगुप्त इनके साहित्यविद्या के गुरु है । ये जन्म से शैव थे किन्तु कालान्तर में वैष्णव हो गए थे । बाद में इन्होने बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया जिसका प्रभाव इनकी परवर्ती रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है । कश्मीर के राजा अनन्त और उनके पुत्र कलश के शासन काल में कवि क्षेमेन्द्र का मुख्य काल मना गया है । उन्होने भरतमञ्जरी की रचना 1037 ई. में की तथा दशावतारचरित की रचना 1066 ई. में की । इस प्रकार उनका काल 1000 ई. माना जा सकता है ।
कवि क्षेमेन्द्र की रचनाओं को चार विभागों के माध्यम से समझा जा सकता है –
महाकाव्य – रामायणमञ्जरी, भारतमञ्जरी, बृहत्कथामञ्जरी, दशावतारचरित तथा अवदानकल्पलता ।
उपदेशात्मक काव्य – कालविलास, समयमातृका, चारुचर्याशतक, सेव्यसेवकोपदेश, दर्पदलन, नर्ममाल, देशोपदेश तथा चतुर्वर्गसंग्रह ।
काव्यशास्त्रीयग्रन्थ – कविकण्ठाभरण, औचित्यविचारचर्चा तथा सुवृत्ततिलकम् ।
प्रकीर्ण – लोकप्रकाशकोश, नीतिकल्पतरु तथा व्यासाष्टक ।
इस प्रकार 19 रचनाए प्राप्त होती है । तथा इनका मृत्यु काल 1075ई. माना गया है ।
मङ्ख/मङ्खक –
संस्कृत साहित्य में श्रीकण्ठचरित महाकाव्य के रचयिता के रुप में मङ्ख कवि सुप्रसिद्ध है । सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्री रुय्यक मङ्ख के साहित्यिक गुरु थे । दोनों गुरु शिष्य कश्मीर नरेश जयसिंह के सभा पंडित थे ।
अतः इनका काल 12वी. शताब्दी का पूर्वार्ध (1100 से 1150 माना जा सकता है ।
कविराज माधवभट्ट –
इनका काल 12वी शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है । ये कदम्ब राजा कामदेव के आश्रित कवि के रुप में भी जाने जाते है । माधवभट्ट ने संस्कृत साहित्य में द्विसंधान काव्य की परम्परा का उदय किया । द्विसंधान काव्य का अर्थ है ऐसा काव्य जो प्रत्येक पद्य में दो अर्थों को प्रदान करने का सामर्थ्य रखे ।
माधवभट्ट ने द्विसंधान काव्य लिखा जिसका नाम राघवपाण्डवीयम् था । इस काव्य के प्रत्येक पद्य से रामायण तथा महाभारत से सम्बद्ध अर्थों की प्राप्ति होती है । माधवभट्ट की उपाधि कविराज थी किन्तु उन्हे कविराज के नाम से ही जाना जाने लगा और यही उनका मुख्यनाम हो गया । कविराज के विषय में पद्य है कि उनकी वक्रोक्ति भी अद्भुत थी –
सुबन्धुर्बाणभट्टश्च कविराज इति त्रयः ।
वक्रोक्तिमार्गनिपुणश्चतुर्थो विद्यते न वा ।।
अर्थात् वक्रोक्ति के प्रयोग में सुबन्धु और बाण के अतिरिक्त कविराज ही सामर्थ्यशाली है अन्य कोई नहीं है ।
श्रीहर्ष –
श्रीहर्ष का नाम माघ और भारवि के समान महान् कवियों में परिगणित होता है । साहित्य की बृहत्-त्रयी रचनाओं में एक रचना श्रीहर्ष की भी है । इनका महाकाव्य नैषधीयचरित संस्कृत साहित्य का अनन्य ग्रन्थ है । इस महाकाव्य में अलंकार और रस के अति आह्लादक पद्य है । यह काव्य विचित्र और सुकुमार दोनों मार्गों को प्रशस्त करने वाला है । यह काव्य अपने कल्पना जन्य वर्णनों की प्रचुरता कारण भारवि और माघ को पीछे छोड देता है । अतः कहा भी गया है – उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारविः ।
श्रीहर्ष ने महाकाव्य में अपना परिचय दिया है । ये कान्यकुब्ज(कन्नौज) नरेश जयचन्द्र के आश्रय कवि थे । इसके अनुसार इनका काल निश्चित रुप से 1150ई. से 1200ई. रहा है । महाकाव्य में इनके द्वारा रचित ग्रन्थों का भी विवरण प्राप्त होता है ।
श्रीहर्ष की रचनाएं –
नैषधीयचरितम् , स्थैर्यविचारप्रकरण, श्रीविजयप्रशस्ति, खण्डनखण्डखाद्य, गौडोर्वीशकुलप्रशस्ति, अर्णववर्णन, छिन्दप्रशस्ति, शिवशक्तिसिद्धि तथा नवसाहसांकचरितचम्पू ।
पट्टनवंशीय कवि वस्तुपाल –
कवि वस्तुपाल गुजरात के निवासी थे । इनका काव्य परम्परागत काव्यों के अन्तर्गत आता है । जिसमें रामायण, महाभारत तथा पुराणों के कथानक के आधार पर काव्य रचना की जाती है । कवि वस्तुपाल चालुक्य नरेश वारधवल के प्रधान मन्त्री थे । अतः इनका समय 1219ई. से 1241ई. माना गया है । ये उदारता के लिए प्रसिद्ध थे । कवियों के आश्रयदाता तथा अनेकों काव्यों के रचयिता वस्तुपाल गिरनार क्षेत्र में 1241 ई. में सुरधाम को प्रस्थित हुए ।
कवि वस्तुपाल जैन मतावलम्बी थे तथापि उन्होनें वैष्णवभाव के ग्रन्थ की रचना कर विशालहृदयता का परिचय दिया है । उनके ग्रन्थ का नाम नरनारायणानन्द है । जिसमें अर्जुन के रुप में नर तथा कृष्ण के रुप में नारायण की मैत्री का वर्णन है ।
वेदान्तदेशिक –
इनका एक ऐर नाम प्रचलित है – वेङ्कटनाथ । इन्होने शताधिक छोटे-बडे़ ग्रन्थों की रचना की । ये रामानुजसम्प्रदाय के समर्थक थे । ये मूलतः काञ्ची के निवासी थे और इन्हे तार्किक सिंह की उपाधि प्राप्त है । इनकी शताधिक रचनाओं की संख्या सवा सौ बतलाई जाती है । जिनमें यादवाभ्युदय महाकाव्य सुप्रसिद्ध है । इस महाकाव्य में भगवान् कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है । इसके अतिरिक्त तत्वमुक्ताकलाप (रामानुजदर्शन), हंस-सन्देश (दूतकाव्य), पादुकासहस्रम्(राम की खडाऊँ की स्तुति), संकल्पसूर्योदय (प्रतीकात्मक नाटक) तथा शतदूषणी (शांकर वेदान्त पर 100 दोषों का आरेप करने वाला दार्शनिक ग्रन्थ) प्रसिद्ध है ।
इनके अतिरिक्त अन्य भी परम्परागत काव्य हैं । जैसे –
9वी. शताब्दी के वासुदेव द्वारा रचित युधिष्ठिरविजयम् ।
12वी. शताब्दी के कृष्णलीलाशुक (बिल्वमंगल) द्वारा रचित गोविन्दाभिषेक
1185ई. के कविकर्णपूर द्वारा रचित पारिजातहरण
1260ई. के अमरचन्द्र द्वारा रचित बालभारतम्
1320ई. के वासुदेव द्वारा रचित नलोदय
1330ई. के साकल्यमल्ल द्वारा रचित उदारराघवम्
1400ई. के वामनभट्ट बाण द्वारा रचित रघुनाथचरित तथा नलभ्युदय
1450ई. के शिवसूर्य द्वारा रचित पाण्डवाभ्युदय
1460ई. के सलुवनरसिंह द्वारा रचित रामाभ्युदय
1650ई. के नीलकण्ठ द्वारा रचित शिवलीलार्णव तथा गङ्गावतरण
1660ई. के श्रीनिवास द्वारा रचित भूवराहविजय
इसके अतिरिक्त कुछ आधुनिक रचनाकार भी है जिन्होने संस्कृत साहित्य को गौरवान्वित किया है । इनका रचना काल 20वी. शताब्दी है । इनके नाम तथा रचनाए निम्नलिखित हैं-
बदरीनाथ झा – राधापरिणय
उमापतिद्विवेदी – पारिजातहरण
रामसनेही दास – जानकीचरितामृत
रेवाप्रसाद द्विवेदी – सीताचरित
अभिराजराजेन्द्रमिश्र – जानकी जीवनम्
सम्प्रति अतिगौरव शंका के कारण जैन, प्राकृत, प्रकीर्ण तथा ऐतिहासिक काव्यों के विवरण अग्रिम शृंखला में प्राप्त होंगे ।